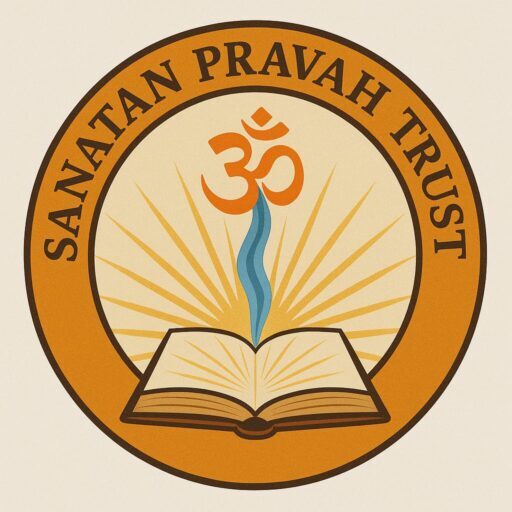अष्टांग योग – सम्पूर्ण जीवनशैली की ओर एक पथ
योग भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है, जिसे महर्षि पतंजलि ने सूत्रबद्ध किया। पतंजलि योगसूत्र में वर्णित “अष्टांग योग” का अर्थ है – योग के आठ अंग, जो व्यक्ति को आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का सम्पूर्ण मार्ग है। अष्टांग योग का उद्देश्य है – चित्त की वृत्तियों का निरोध, जिससे व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सके।
1. यम (नैतिक अनुशासन):
यम अष्टांग योग का प्रथम अंग है, जो व्यक्ति के सामाजिक आचरण से संबंधित है। यह पाँच प्रकार के होते हैं:
- अहिंसा – किसी भी जीव के प्रति हिंसा न करना।
- सत्य – विचार, वाणी और कर्म में सत्यता।
- अस्तेय – चोरी या किसी की वस्तु का अनुचित उपयोग न करना।
- ब्रह्मचर्य – इन्द्रियों पर संयम रखना।
- अपरिग्रह – अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना।
यम हमें सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक आचरण सिखाते हैं।
2. नियम (व्यक्तिगत अनुशासन):
नियम व्यक्ति के आत्म-संयम और निजी जीवन से संबंधित हैं। यह भी पाँच प्रकार के होते हैं:
- शौच – शरीर और मन की शुद्धता।
- संतोष – वर्तमान में संतुष्ट रहना।
- तप – कठिनाइयों में भी धैर्य एवं आत्मनियंत्रण।
- स्वाध्याय – धर्मग्रंथों का अध्ययन और आत्म-चिंतन।
- ईश्वर प्रणिधान – ईश्वर में आस्था और समर्पण।
नियम आत्म-विकास की दिशा में पहला कदम है।
३.आसन (शारीरिक अभ्यास):
आसन शरीर को स्वस्थ, स्थिर और सशक्त बनाने का साधन है। पतंजलि के अनुसार, “स्थिरसुखमासनम्” – वह आसन जो स्थिर और सुखद हो। आधुनिक युग में योगासनों की महत्ता बढ़ गई है, क्योंकि ये तनाव, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि समस्याओं में सहायक हैं। आसन से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और ध्यान के लिए अनुकूल स्थिति बनती है।
4. प्राणायाम (श्वास नियंत्रण):
प्राणायाम का तात्पर्य है – प्राण (जीवन ऊर्जा) का नियंत्रण। यह श्वास की गति को नियंत्रित कर मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाता है। इसके चार मुख्य चरण हैं – पूरक (श्वास लेना), कुम्भक (रोकना), रेचक (छोड़ना), और शून्यक। प्राणायाम से तनाव कम होता है, चित्त शुद्ध होता है और ध्यान के लिए मानसिक तैयारी होती है।
ध्यान से मानसिक शांति, आत्म-चिंतन और आत्म-ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह सभी मानसिक विकारों को दूर करने का उपाय है।
5. प्रत्याहार (इन्द्रिय संयम):
प्रत्याहार का अर्थ है – इन्द्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुख करना। यह ध्यान की दिशा में पहला गम्भीर कदम है, जहाँ साधक अपनी इन्द्रियों को वश में रखकर मन को भीतर की ओर केंद्रित करता है। आज के डिजिटल युग में, जहाँ इन्द्रियाँ बाहरी आकर्षणों में उलझी रहती हैं, प्रत्याहार की अत्यधिक आवश्यकता है।
6. धारणा (एकाग्रता):
धारणा वह स्थिति है जब मन किसी एक विषय या वस्तु पर स्थिर हो जाता है। यह एक बिन्दु पर चित्त की एकाग्रता का अभ्यास है, जैसे – किसी मंत्र, मूर्ति, प्रकाश, या स्वांस पर ध्यान केंद्रित करना। धारणा से चित्त की चंचलता कम होती है और ध्यान के लिए मार्ग प्रशस्त होता है।
7. ध्यान (मेडिटेशन):
ध्यान धारणा का परिष्कृत रूप है। इसमें साधक निरंतर उस एक बिन्दु पर ध्यान लगाता है, जिससे धीरे-धीरे ‘कर्ता’ का बोध समाप्त होने लगता है।ध्यान से मानसिक शांति, आत्म-चिंतन और आत्म-ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह सभी मानसिक विकारों को दूर करने का उपाय है।
8. समाधि (परम स्थिति):
समाधि अष्टांग योग का अंतिम और सर्वोच्च चरण है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक आत्मा और परमात्मा में पूर्ण एकत्व का अनुभव करता है।
यह निर्विकल्प स्थिति है – जहाँ विचार, अहंकार
और द्वैत मिट जाते हैं। समाधि की स्थिति में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अष्टांग योग न केवल साधकों के लिए, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक जीवन पद्धति है। यह मन, शरीर और आत्मा की एकता स्थापित करता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहाँ मानसिक तनाव और असंतुलन आम हो चुके हैं, अष्टांग योग एक स्थायी समाधान प्रदान करता है। यदि व्यक्ति इसका नियमित अभ्यास करे तो न केवल वह एक बेहतर स्वास्थ्य पा सकता है, बल्कि आत्म-ज्ञान और शांति की ओर भी अग्रसर हो सकता है।